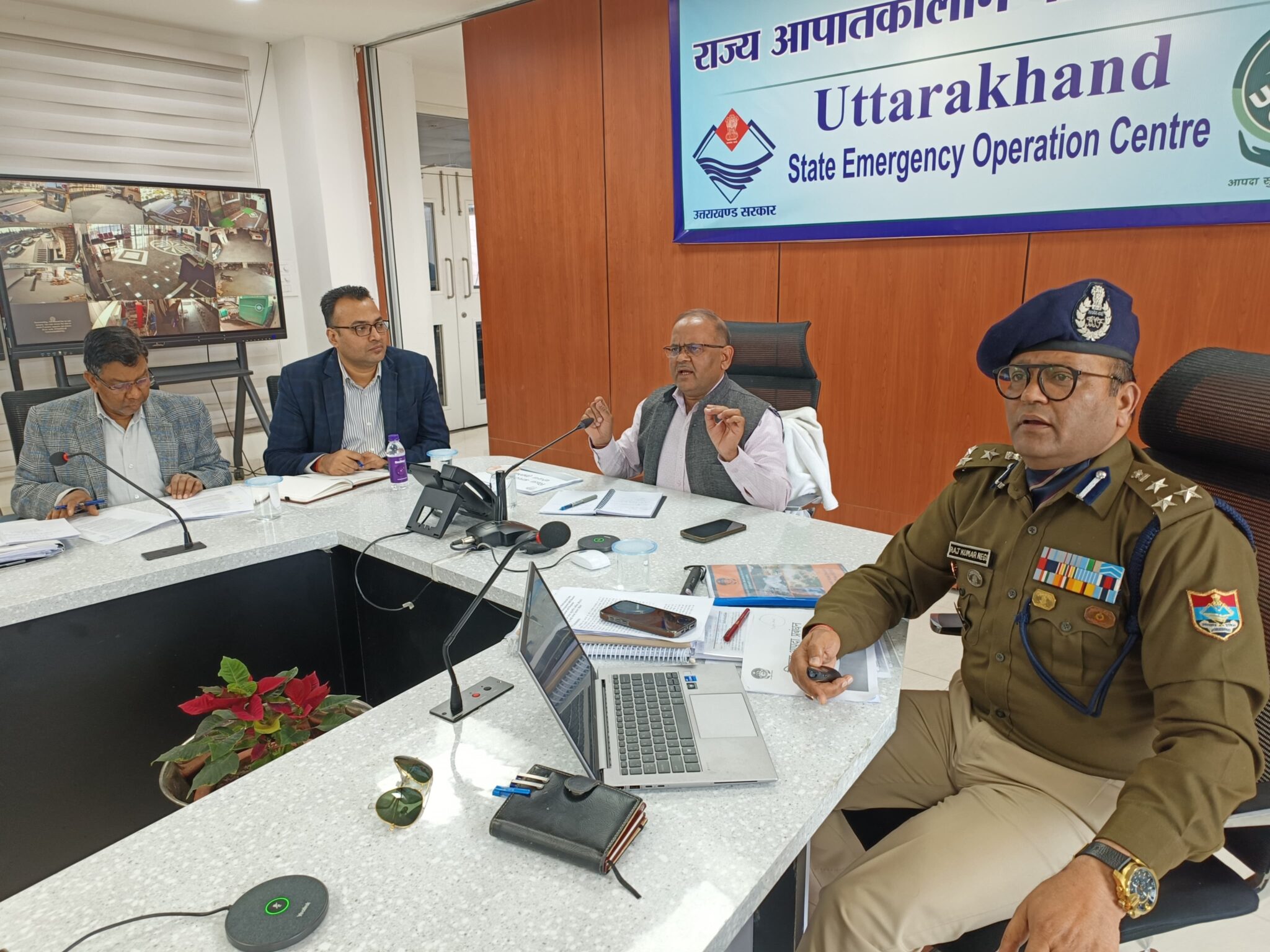देहरादून 5 अगस्त । सिडार संस्था और दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र की ओर से मानव-तेंदुए संघर्ष के सामाजिक-पारिस्थितिक और भू-स्थानिक आयाम पर एक गोलमेज बैठक का आयोजन केन्द्र के सभागार में किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष हमें यह यह स्वीकार करना होगा कि मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को एक सच्चे सह-अस्तित्व के लिए मानवें और जानवरों, दोनों की ज़रूरतों और कमज़ोरियों को समझना और उनका समाधान करना आवश्यक है।
सिडार संस्था और दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र की ओर से मानव-तेंदुए संघर्ष के सामाजिक-पारिस्थितिक और भू-स्थानिक आयाम पर एक गोलमेज बैठक का आयोजन केन्द्र के सभागार में किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष हमें यह यह स्वीकार करना होगा कि मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को एक सच्चे सह-अस्तित्व के लिए मानवें और जानवरों, दोनों की ज़रूरतों और कमज़ोरियों को समझना और उनका समाधान करना आवश्यक है।
पारिस्थितिकी विज्ञानी प्रोफेसर एस.पी. सिंह और सिडार के प्रभारी डॉ. विशाल सिंह ने गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत यह कहते हुए की कि पारिस्थितिकी अनुप्रयोग और प्रबंधन के बारे में अधिक विचार करती है। हमें जानवरों को भी स्थान और जनसंख्या का एक हिस्सा मानना चाहिए। शहरीकरण के कारण मनुष्यों और जानवरों के बीच भौतिक अलगाव बढ़ रहा है।
इसके बाद कार्लटन कवश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीप्तो सरकार द्वारा युगांडा के किबाले राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण पर प्रस्तुति दी गई उन्होनें मानव-वन्यजीव संघर्ष पर नज़र रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल और एक सफल संरक्षण कार्यक्रम कैसा दिखता है और यूरोप, अमेरिका के मुकाबले भारत में समुचित वन्य संरक्षण अभ्यास असफल क्यों रहे हैं इस पर बात रखी। उन्होनें सह-अस्तित्व का विचार पर जोर देते हुए सह-अस्तित्व में रहने की बात का समर्थन किया।
यूपीईएस के टाइपक्राफ्ट इनिसिऐटिव एम.आर.इशान खोसला ने वन से वनवास पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया।लोक एवं जनजातीय कलाकारों के साथ सहयोगात्मक कार्य और पशुओं के अस्तित्व पर बात रखी। उन्होने कहा कि वाहन को जानवरों के रूप में चित्रित करना संभवतः उन्हें शोषण से बचाने के लिए किया गया था। लोक और आदिवासी कलाकार आमतौर पर जानवरों के साथ काम करते हैं।वनों और वन्य जीवों के सवाल पर उन्होने कहा कि आजकल वन क्षेत्र लगभग न के बराबर बचा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पवित्रता एक प्रमुख क्यूरेटोरियल थीम है। प्रजातियाँ तेज़ी से लुप्त हो रही हैं, हमारी प्रगति उनके आवासों को नुकसान पहुँचा रही है।
हावर्ड विश्वविद्यालय वाशिंगटन,डीसी की डॉ. हिमानी नौटियाल ने कहा कि कुछ नए विचार विकसित करने की आवश्यकता है। इसका असर इंसानों और जानवरों, दोनों पर पड़ रहा है। तेंदुओं द्वारा इंसानों को मारना कोई नई घटना नहीं है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कई बैठकें होती हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, शायद इसलिए कि हम ठीक से सहयोग नहीं कर रहे हैं। किसी छोटी अवधि की परियोजना के बजाय दीर्घकालिक परियोजना पर काम करना अणिक प्रभावी हो सकता है। तेंदुओं द्वारा इंसानों पर हमला करने पर, कोई उपाय सोचने और सफल प्रयासों पर गौर करना जरूरी है।
संघर्ष क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों का समर्थन कैसे किया जा सकता है? पूरी बात हमेशा मुआवज़े पर केंद्रित हो जाती है।
वक्तओं ने चर्चा के दौरान ग्रामीणों को जानवरों के हमलों से बचने के लिए सुरक्षात्मक ढाँचों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने, रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकने, ऐप-आधारित संरक्षण प्रणालियों का उपयोग और प्रचार स्थानीय लोगों को वन्यजीवों के बारे में सचेत करने के लिए किये जाने जैसे अहम सवाल भी रखे। कहा गया कि स्थानीय लोगों की अपनी प्रबंधन योजनाएँ पर उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने और उन पर अमल करने की आवश्यकता है। जानवरों के व्यवहार के लिए बहुत सारे नमूनों की आवश्यकता होती है और अब तकनीक भी उपलब्ध है।
बैठक में इनके अलावा तेंदुओं के रहस्य को उजागर करने, नई पीढ़ी को किस तरह शिक्षित कर सके ,आवास, पूर्व चेतावनी प्रणाली आदि का निर्माण, हॉटस्पॉट की भेद्यता, नागरिक विज्ञान, वन विभाग की क्षमता, सामुदायिक सहयोग जैसे महत्वर्पूएा बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई।
बैठक में बिजू नेगी, डॉ.मालविका चौहान, रेनू सुयाल,निधि सिंह, कुलदीप उनियाल, अंलति भरतरी,डॉ. प्रदीप मेहता, अश्विनी पुरी, पंकज जोशी और अमित भाकुनी सहित कई वक्ताओ ने अपने विचार रखे।